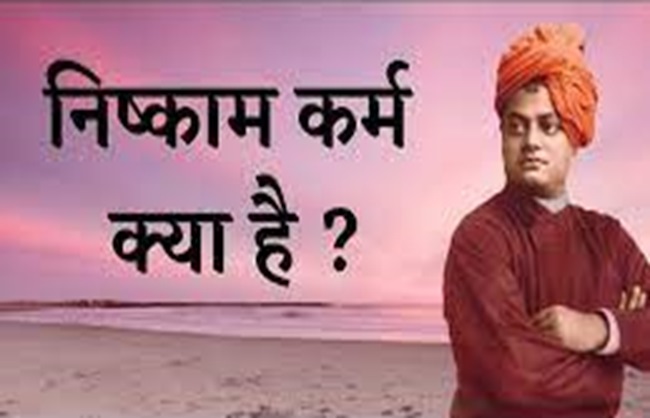अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में सुख और दुख का अनुभव करना बुद्धि की प्रतिक्रिया है। लाभ और हानि मन की कल्पनायें हैं जिससे किसी चीज को लेकर खुशी और गम होना स्वाभाविक है। लालसा किये गए सामान और वस्तु हासिल करने पर खुशी और नहीं मिल पाने पर गम होना स्वाभिवक है। भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं मनुष्य के जीवन में इस प्रकार की विषम परिस्थितियां पैदा होने पर हमेशा मन को संतुलित रखना चाहिये। परन्तु इसके लिए अभ्यास और सतत जागरूकता की जरूरत होती है। ठीक उसी प्रकार जब कोई समुद्र में स्नान करना चाहता है तो उसको समुद्र स्नान करने की कला मालूम होनी चाहिए। नहीं तो समुद्र की उफनती लहरें व्यक्ति को परेशान कर देगी और अंततः वह डूब जाएगा। परन्तु जो व्यक्ति यदि ऊंची लहरों के नीचे झुकने और छोटी लहरों पर सवार होने की कला जानता हो, तो वह बखूबी समुद्र में स्नान का आनन्द उठा सकता है।
यदि कोई व्यक्ति समुद्र की लहरें शान्त होने की आशा करता है और सोचता है कि लहरें शांत हो जाएगी तो स्नान करेंगे तो कष्ट नहीं होगा। तो यह अपनी सुविधा के लिये व्यक्ति द्वारा समुद्र को उसके स्वरूप को त्याग करने के आदेश देने के जैसा है। पर अज्ञानी व्यक्ति जीवन में यही चाहता है कि, किसी प्रकार समस्यायें उसके सामने न आयें जो बिलकुल असम्भव है। जीवन के समुद्र में सुख-दुख, लाभ -हानि और जय-पराजय की लहरें उठना अनिवार्य है। अन्यथा गति हीनता के चलते जीवन निरर्थक हो जाता है और पूर्ण गति हीनता ही मृत्यु है। यह जीवन एक उफनते लहरों से भरे समुद्र के जैसा है, जिसमें काफी हलचल होती रहती है, जो कभी ऊपर-नीचे तो कभी शांत रहती है। उसमें उठती ऊंची- नीची लहरों के प्रहार से विचलित हुये बिना जीवन जीने की कला हमें सीखनी चाहिये। इन उठती गिरती लहरों के साथ सामंजस्य स्थापित कर लेने से ही इसकी सतह पर इधर- उधर बहते जाना सम्भव है न कि उस सर्च लाइट के पोल जैसा जो लहरों के बीच एक ही जगह खड़ा रहता है।
भगवान श्रीकृष्ण, अर्जुन को युद्ध के लिये प्रेरित करते हुए समत्व भाव का महत्व बताते हैं। क्योंकि कई बार कर्म में संलग्न व्यक्ति अपनी ही नकारात्मक सोच का शिकार बन जाता है और जीवन के आनंद से वंचित रहता है और कष्ट का अनुभव करता है। मन के इस समभाव से ही व्यक्ति वास्तविक स्फूर्ति और प्रेरणादायक जीवन का आनंद लेता है और ऐसा व्यक्ति ही उपलब्धियां भी हासिल करता है, जो सच्ची सफलता की आभा से दैदिप्यमान होता है। यह सर्वविदित है कि किसी भी कार्य क्षेत्रें में जो कर्म स्फूर्ति और प्रेरणा से भरपूर होते हैं, उनकी अपनी ही एक चमक होती है। उसके जैसा कोई दूसरा नहीं होता न ही उसे दोहराया जा सकता है।
जब हम दैवी प्रेरणा के आनन्द से अविभूत होकर कोई कार्य कर रहे होते हैं, तब हमारी कल्पनायें विचार और कर्म अपनी ही निराली सुन्दरता से ओत प्रोत होती है। जीवन में ऐसे कई उदाहरण हैं, जो इसकी सत्यता को उजागर करते हैं जैसे प्रसिद्ध चित्रकार दा विन्सी अपनी श्रेष्ठ कृति मोनालिसा का चित्र दोबारा नहीं बना सकें। भगवान् श्रीकृष्ण ने भी युद्ध के पश्चात् अर्जुन के अनेक विनती करने पर दोबारा गीता सुनाने में अपनी असमर्थता व्यक्त की।
पश्चिमी विचारकों के अनुसार प्रेरणा, कोई संयोग या रहस्यमय घटना है, जिस पर व्यक्ति का कोई नियंत्रण नहीं होता। जबकि भारतीय ऋषि मुनियों या महानुभावों के अनुसार दैवी प्रेरणा का जीवन मनुष्य का वास्तविक लक्ष्य है। जिसे वह अपने आत्म स्वरूप के साथ पूरी तरह तादात्म्य स्थापित करके जी सकता है। और इसका उपाय सिर्फ समत्व भाव का वह जीवन है, जहाँ हम परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना अपने मन और बुद्धि का साक्षी बनकर रहते हैं।
यह अहंकार को भूलने का क्षण है। जब कोई व्यक्ति इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है, तो उसका जीवन सुबह की नरम धूप और नयी किरण के जैसी जगमगाती आभा से भरी होती है। जबकि साधारण व्यक्ति यह सोचते हैं कि, अहंकार या अभिवृत्ति नहीं होने पर कार्य में कुशलता नहीं मिलेगी। हम वह कार्य ही नहीं कर पाएंगे। पर यह गलत अवधारणा है। प्रेरणा की आभा सामान्य सफलता को भी महान उपलब्धि में बदल सकती है।
हमारे ऋषि मुनियों ने योग विकसित किये जिसके अभ्यास से व्यक्ति मन और बुद्धि के बीच जुड़ाव पैदा कर सकता है और समता का भाव विकसित किया जा सकता है। वैदिक काल के लोगों को इसका उचित ज्ञान था और वे इसका अभ्यास कर योगी जीवन जीते थे। इसके माध्यम से उन्होंने असाधारण उपलब्धियां अर्जित कर, राष्ट्र के लिये स्वर्णयुग का निर्माण किया। जिसके चलते हम भारत को सोने की चिड़ियाँ भी कहते हैं।
हम अपने इतिहास को देखते हैं तो इसके कई अप्रतिम उदाहरण मिलते हैं, जैसे भगवान राम के जीवन में कितने संघर्ष आए और वे सभी परिस्थितयों में समभाव स्थापित कर परिस्थियों की स्वस्थिति के रूप में परिवर्तित करते हुए उसे स्वीकार कर, उस पर विजय प्राप्त किए। लोक जगत के लिए पूजनीय हुए। भारत जैसे देश में वैदिक काल में निश्चित ही आस्तिक दर्शन प्रचलित रहा होगा। आज भी इसकी प्रासंगिकता और उपयोगिता जीवन के सभी क्षेत्रें में उतनी ही है।
परिस्थितियों का मूल्यांकन सिर्फ आध्यात्मिक दृष्टिकोण से करना ठीक नहीं बल्कि, जीवन की हर एक परिस्थिति या चुनौती को आध्यात्मिक दृष्टिकोण के साथ-साथ बुद्धि के स्तर पर तर्क व मन के स्तर पर नैतिकता और भौतिक स्तर पर परम्परा तथा सामाजिक रीति- रिवाज के अनुसार भी करना जरूरी है। इन सब के माध्यम से बिना किसी विरोधाभास के यदि किसी एक सत्य का संकेत मिलता है तो निश्चय ही वह दिव्य मार्ग है जिस पर व्यक्ति को किसी भी कीमत पर चलने की कोशिश करनी चाहिये।
केवल नैतिकता की भावना से युद्ध की ओर देखने से अर्जुन उस परिस्थिति के सही स्वरुप को समझ नहीं सके। अपने परिवारजनों और अग्रजों तथा जिन्होंने उन्हें पाला पोशा, बड़ा किया और शिक्षा दी, उनके विरूद्ध युद्ध करना नैतिकता के आधार पर उन्हें उचित नहीं जान पड़ा। क्योंकि भावावेश में उनका मन भ्रमित होने के चलते अन्य दृष्टिकोणों पर विचार नहीं कर सका जिससे वह पुनः संतुलित और संयमित हो सकते थे। अपने विचलित मन की अवस्था में मनुष्य को ईश्वर या ज्ञानीजन की शरण लेनी चाहिए। अर्जुन भी ऐसे अवसर पर भगवान कृष्ण की शरण में जाते हैं। श्रीकृष्ण उनको मार्गदर्शन करते हुए जीवन के सभी दृष्टिकोणों को उसके सामने प्रस्तुत करते हैं। भगवान श्रीकृष्ण मनुष्य को प्राप्त विवेकशील बुद्धि की भूमिका निभाते हैं, जो हमारे देहरूपी रथ का योग्य सारथी है। मन के समत्व भाव में रहने से जीवन की वास्तविक सफलता निश्चित होती है। कर्मयोग की भावना से कर्म करते हुये जीवन जीने पर अन्तकरण की शुद्धि प्राप्त होती है।
इसलिए हर किसी को फल की इच्छा किये बिना, कर्म करने चाहिए और बिना विचलित हुए हर परिस्तिथि का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तभी जीवन में सफलता प्राप्त होती है।लौनों से और अधिक रोमांचक लग रहा है। और उस समय कंप्यूटर उसकी पूरी दुनिया बन जाता है। फिर एक दिन हम पाते हैं कि उसे कंप्यूटर गेम में भी कोई दिलचस्पी नहीं है। क्योंकि उसकी इच्छा कहीं और शिफ्ट हो गई है। उसके लिए अब पुरानी चाहत व्यर्थ हैं। इस प्रकार वह एक पूर्ण वयस्क के रूप में विकसित होता है और अब दूसरे प्रकार का जुनून हैं-जैसे धन शक्ति, पद, स्थिति आदि की इच्छाएं।
इस तरह हम ऊँची इच्छाओं की ओर बढ़ते जाते हैं। इस स्तर पर पहुंचने के बाद, हम केवल यथास्थिति बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन अभी भी एक लम्बा सफर तय करना बाकी है। यदि हम दुनिया से अलग किसी चीज की कल्पना कर सकते हैं तो हम उस परिप्रेक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं जो हमें और भी आगे बढ़ने को प्रेरित करेगा।
हम सभी में परमात्मा की वह आंतरिक पुकार है जो हमें बताती है कि जीवन से परे कुछ होना चाहिए जिसे हम नहीं जानते हैं। और हमारे अंदर वह नैसर्गिक खोजपूर्ण भावना है जिससे उस सत्य को खोजने के लिए जब हम इस यात्र पर निकलते हैं तो पाते हैं कि कोई भी साथ नहीं है। लोग हमारे विश्वास का मजाक उड़ाते हैं और वे कभी-कभी सत्य की खोज के इस मार्ग में बाधक भी बनते हैं। वे सोचते हैं कि हम भटक गए हैं जबकि वास्तव में वे ही हैं जो भटके हुए हैं!
एक बार जब हम अकेले सत्य का अनुसरण करने में सक्षम हो जाते हैं, तो हम एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं, जहां अन्य लोगों के साथ तालमेल बिठाने लगते हैं। पर हमने अभी तक उच्च स्तर का अनुभव नहीं किया है। हम सांसारिक सुखों से संतुष्ट नहीं रह सकते हैं और आध्यात्मिक आनंद तक हमारी पहुंच नहीं बनी है। ऐसा लगता है जैसे नो-मैन्स लैंड में पहुंच गए हैं। हालाँकि साधक को फिर भी दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ना चाहिए।
यदि ऐसा किया जाता है तब एक ईश्वरीय संकेत मिलता है कि हम सही रास्ते पर हैं। हमारे जीवन में चीजें सही होने लगती हैं। इस नए पकड़े गए सिरे से दृढ़ विश्वास के साथ हम तब तक आगे बढ़ते रहते हैं जब तक हम प्राप्ति तक नहीं पहुंच जाते। भारत में प्रत्येक पीढ़ी में एक महान द्रष्टा उभरा है, जो हमें नई दुनिया के बारे में बताता है- चेतना के चौथे स्तर का अनुभव। लेकिन चूंकि हम नहीं समझते हैं, हमें आश्चर्य होता है कि वह किस बारे में बात कर रहा है। वह वापस क्यों आए और हमसे बात क्यों करें? क्योंकि उनके पास अपने अनुभव के आनंद और शांति को साझा करने के अलावा और कोई इरादा नहीं है।
वह हमें सच बताता है। प्रारंभ में हम शास्त्रें के गहरे महत्व को नहीं समझ सकते हैं, लेकिन समय के साथ हमें इसकी सत्यता का एहसास होता है। यह गुरु-शिष्य परंपरा है – जो आदिकाल से जारी है। आध्यात्मिक विकास क्रमिक होना चाहिए। जब हम इच्छाओं से भरे होते हैं तो उन्हें अचानक नहीं छोड़ सकता। वास्तव में कोई भी मनुष्य इच्छाओं को बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। हम जो कुछ भी कर सकते हैं, वह कुछ अधिक मूल्यवान हो, कुछ ऐसा जो अधिक संतोषजनक हो, जो हम अभी कर रहे हैं उससे अधिक संतुष्टिदायक हो।
यदि हम शारीरिक स्तर पर हैं, तो कोशिश करें और भावनात्मक स्तर पर आगे बढ़ें। एक बार जब भावनात्मक संतुष्टि के आनंद का स्वाद चख लेते हैं तो हमारे अपने पहले के प्राप्त भौतिक सुख तुच्छ लगने लगते हैं। एक बौद्धिक लक्ष्य की ओर बढ़ने पर एक समय भावनात्मक खुशी भी महत्वहीन हो जाती है।
मान लीजिए उन्होंने कहा था, फ्जब कोई मन की सभी इच्छाओं को पूरी तरह से त्याग देता है तो वह एक वास्तविक आत्मा है’’ तो ऐसे में हम सभी गहरी नींद में ही इसके योग्य होंगे। क्योंकि गहरी नींद में कोई इच्छा नहीं होती। लेकिन वह बोध की स्थिति नहीं है क्योंकि उस अवस्था में हमें आत्मा या आत्मा का कोई ज्ञान नहीं होता है। हमें नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पहलुओं में योग्यता प्राप्त करनी चाहिए। आत्मा में तृप्त होने के कारण जब मनुष्य मन की समस्त कामनाओं का पूर्णतः परित्याग कर देता है, तो वह स्थितप्रज्ञ कहलाता है।
विकास हर पहलू में होता है। जब हम केवल स्वाद से ज्यादा स्वच्छता को महत्व देनें लगते हैं, तब अगर कोई हमसे कहता है कि सड़क के किनारे के अमुक स्टाल पर स्वादिष्ट खाद्य मिलता है तो हमारा वहां जाने का मन नहीं करेगा। ऐसी अवस्था में हम जंक फूड पसंद तो करते हैं लेकिन चूंकि स्वास्थ्य की इच्छा पैदा होती हैं अतः तैलीय भोजन के प्रति विरक्ति पैदा होती है- और हम इसका आनंद नहीं लेते हैं। जब हम अच्छे कपड़ों की इच्छा करते हैं तो भड़कीले, खराब फिटिंग वाले कपड़ों पर वापस नहीं जा सकते। जब अनुचित भाषा से परिष्कृत भाषा की ओर बढ़ते हैं, तो अनुचित भाषण पर वापस नहीं जा सकते। वृद्धि, एकदिशीय होती है। एक बार जब हम उच्च स्तर पर पहुंच जाते हैं तो कभी भी निचले स्तर पर वापस नहीं आ सकते हैं।
श्रीमद्भगवद् गीता हमें यह आश्वासन देती है, ‘यद गत्वा न निवर्तन्ते।’ अर्थात्- उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद, वापस नहीं जाना है। जब हम किसी भावना को बहुत दृढ़ता से महसूस करते हैं तो हम पाते हैं कि उसे व्यक्त करने को शब्द अपर्याप्त हैं। क्रोधित व्यक्ति अजीबोगरीब बातें कहता है क्योंकि भावनाओं के आवेग को संप्रेषित करते समय भाषा लड़खड़ा जाती है। जब हम किसी बौद्धिक विचार को समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं तो यह और भी मुश्किल हो जाता है।
जटिल, अमूर्त वैज्ञानिक अवधारणाओं को समझाना मुश्किल है। यहाँ पर उस आत्मा के बारे में बताने का प्रयास है जो कि बुद्धि से परे है और इसे संप्रेषित करने के लिए सीमित, शब्दों का उपयोग किया जा रहा है। भगवद् गीता में भगवान श्रीकृष्ण द्वारा उठाए गए कार्य की प्रकृति इतनी विशाल है और वे इसे कितना अद्भुत अनुभव कराते हैं इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन जब कोई मन को भौतिक आकर्षणों से दूर करना सीखता है और इंद्रियों की इच्छाओं को त्याग देता है, तो वह आत्मा के आंतरिक आनंद के संपर्क में आता है, और दिव्य रूप से स्थित हो जाता है। कंठोपनिषद् में तो यहाँ तक कहा गया है कि जिसने कामनाओं का त्याग कर दिया वह ईश्वर के समान हो जाता है।
वस्तुतः यह विषय बड़ा गहन और जीवन में साकारित करने के लिए कठिन जरूर है। पर अगर मनुष्य इस रास्ते पर चलने का अभ्यासपूर्वक प्रयत्न करते हैं तो भगवद गीता कटिबद्ध है कि हम अपने जीवन का उद्धार स्वयं करने में सक्षम हैं। प्रयास करना हमारा काम है और उस प्रयास के ही अनुपात में परिणाम रूपी फल पर हमारे नाम की मोहर लगाकर हमारे जीवन को उत्कृष्ट करना भगवान का काम है। यदि हम अपने जीवन को सुसंस्कृत बनाने के लिए तत्पर होंगे तो ईश्वरीय मदद हमेशा तैयार मिलेगी और यह श्रीमद्भगवद् गीता के माध्यम से ईश्वर का आहवान है।
 Narvilnews Whole world at one eyesight
Narvilnews Whole world at one eyesight