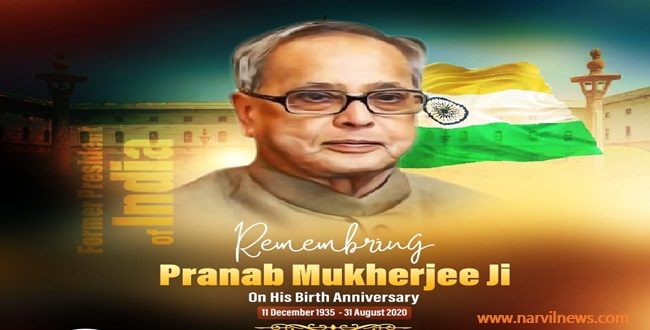पांडुरंग वामन काणे, (भारतरत्न 1963)
(जन्म-७ मे १८८०, मृत्यु- १८ एप्रिल १९७२)
“जितना दंड क्रूर होगा, जुर्म भी उतना ही क्रूर होता जाएगा।” एक सरकारी विधेयक का विरोध करते हुए पांडुरंग वामन काणे ने यह वाक्य कहा था।
महाराष्ट्र प्रदेश के रत्नागिरि नाम के ज़िले की धरती ने अनेक रत्नों को जन्म दिया है। लोकमान्य बालगंगाधर तिलक, राजनेता गोपालकृष्ण गोखले, न्यायमूर्ति रानाडे, आचार्य विनोबा भावे और पांडुरंग वामन काणे इसी रत्नागिरि की उपज हैं। इन सभी ने अपने-अपने क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान बनाया। संस्कृत के अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्रकांड पंडित, प्रसिद्ध विधिवेत्ता और सांसद पांडुरंग वामन काणे का जन्म 7 मई, 1880 को रत्नागिरि के दापोली ग्रामवासी एक चितपावन परिवार में हुआ था। उनके पितामह शंकरराव संस्कृत के विद्वान तो थे ही, साथ में कुशल वैद्य भी थे। उनके पिता वामनराव ने पहले कुछ समय पुरोहिताई का कार्य किया, फिर लीक से हटकर वकालत करनी शुरू कर दी थी।
पांडुरंग का जन्म उनकी ननिहाल में हुआ था, जो चिताली परिवार था। काणे और चिताली परिवारों में वैदिक शिक्षा का प्रचलन था। बालक पांडुरंग पर भी आरम्भ से ही संस्कृत शिक्षा पर जोर दिया गया। दापोली में ही शिक्षा आरम्भ की और वहीं के एस.पी.जी. हाईस्कूल से 1897 में मैट्रिक परीक्षा पास की। आगे की शिक्षा के लिए उन्हें बम्बई जाना था, किन्तु उन दिनों बम्बई में प्लेग फैला हुआ था। इसलिए बम्बई जाना नहीं चाहते थे और शिक्षा की हानि भी सहन नहीं थी । बम्बई स्थित विलसन कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ. मैकिकन को अपनी समस्याओं और शिक्षा में व्यवधान न पड़ने की अपनी बात से भी अवगत कराया और प्रार्थना की कि विलसन कॉलेज में प्रवेश दे दिया जाए। डॉ. मैकिकन ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। उन्हें एक सत्र के लिए घर पर ही पढ़ाई करते रहने की अनुमति भी दे दी गई। परीक्षा आदि से सम्बन्धित अन्य समस्याओं को समय पर विश्वविद्यालय से सुलझा लेने का आश्वासन अलगे से दे दिया।
1901 में पांडुरंग वामन काणे ने बी.ए. पास किया। उन्हें भाऊदाजी संस्कृत पुरस्कार भी तभी प्रदान किया गया। इससे पूर्व भी संस्कृत के मेधावी छात्र होने के कारण कई छात्रवृत्तियां मिल चुकी थीं। बी.ए. कर लेने के बाद उन्हें विलसन कॉलेज में ही दो वर्षों के लिए दक्षिण फेलोशिप मिल गई, जिसके सहारे उन्होंने क़ानून भी पढ़ना शुरू कर दिया। 1902 में एल.एल.बी. की प्रथम परीक्षा में प्रथम श्रेणी में सफल घोषित हुए। अगले वर्ष 1903 में संस्कृत व अंग्रेज़ी में एम.ए. भी कर लिया और वेदान्त पुरस्कार प्राप्त किया। वकालत वह करना नहीं चाहते थे। इसलिए अध्यापन कार्य के लिए उन्होंने डॉ. मैकिकन से शिक्षा विभाग में सिफ़ारिश करने का अनुरोध किया था। उनके चेहरे पर चिन्ता और निराशा छा गई। उन दिनों ब्रिटिश सरकार चितपावनों के सम्बन्ध में अच्छी राय नहीं रखती थी। रानाडे, तिलक आदि सभी चितपावन थे, जिन्होंने देश के स्वतन्त्रता आन्दोलन में अपनी उग्र रणनीति से सरकार की नींद हराम कर दी थी।
फिर भी डॉ. मैकिकन के प्रयासों से पांडुरंग को 60 रुपए प्रतिमाह के वेतन पर रत्नागिरि में अध्यापक की नौकरी मिल गई। वहां उन्हें कई विषय पढ़ाने पड़ते थे। शिक्षा के क्षेत्र में जब पांडुरंग पहुंचे, तो उन्होंने शिक्षक की परीक्षा दी और पूरी बम्बई प्रिज़िडेंसी में प्रथम श्रेणी में पास हुए। अगले वर्ष विभागीय परीक्षा में भी बैठे और सफलता प्राप्त की। इससे उन्हें शिक्षा विभाग में सहायक शिक्षा निरीक्षक का पद मिल गया, परन्तु उन्होंने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया, क्योंकि तब उन्हें अपने शोधकार्य के लिए पर्याप्त समय न मिल पाता।
1907 में पांडुरंग बम्बई स्थित एलफिन्स्टन हाईस्कूल में स्थानान्तरित कर दिए गए। वहां उन्हें संस्कृत का मुख्य अध्यापक बनाया गया। शोध कार्य वहां भी जारी रहा। इस बार उनका विषय था, प्राचीन भारतीय साहित्य, जिसके शोध पर वी.एन. मांडलिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1908 में काणे ने एल.एल.बी. का दूसरा हिस्सा भी पास कर लिया।
अगले वर्ष एक सत्र के लिए प्रोफ़ेसर एस. आर. भंडारकर के रिक्त स्थान पर अध्यापन कार्य मिल गया। पूना के डैकन कॉलेज में संस्कृत के एक प्राध्यापक के पद का सृजन किया गया और पांडुरंग वामन काणे के लिए सिफ़ारिश भी की गई। काणे उस पद के लिए पूरी तरह योग्य थे, फिर भी उनकी उपेक्षा की गई। उनके आत्मसम्मान को आघात पहुंचा और उन्होंने चार वर्ष सेवा करने के पश्चात सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। एल. एल. बी. वह कर चुके थे, परन्तु इतने से भी उन्हें सन्तोष नहीं हुआ और उन्होंने हिन्दू और मुस्लिम क़ानून जैसे गहन विषयों को लेकर एल. एल. एम. किया।
अन्ततः काणे को उनका खोया हुआ सम्मान पुनः प्राप्त हुआ। बम्बई विश्वविद्यालय का ध्यान क़ानून में पांडुरंग के अपार ज्ञान की ओर गया और उन्हें विश्वविद्यालय की ओर से भाषण देने के लिए आमन्त्रित किया गया। इसका विषय था ‘संस्कृति और सहयोगी भाषाएं’। उनके विद्वत्तापूर्ण भाषण से अधिकारी वर्ग अत्यन्त प्रभावित हुआ और उन्हें सौ रुपए प्रतिमास की दो वर्षों की शोध छात्रवृत्ति प्रदान की गई। तब वह केवल तीस वर्ष के थे और यह 1913 की बात थी। इस बार शोध का विषय था, ‘महाराष्ट्र का प्राचीन भूगोल’। व्यापक अध्ययन के बाद उन्होंने इस विषय पर अपना शोधकार्य सफलता के साथ पूरा किया। इसी शोधकार्य से प्रभावित होकर प्रोफ़ेसर भंडारकर के रोगग्रस्त हो जाने के बाद उनके रिक्त स्थान पर पांडुरंग को नियुक्त किया गया।
विलसन कॉलेज से निवृत्त होते ही उन्हें राजकीय कानून विद्यालय में कानून पढ़ाने का कार्य मिल गया। इसे उन्होंने अगले छह वर्ष तक कुशलता के साथ निभाया। काणे का संस्कृत के प्रति अनुराग कभी लुप्त नहीं हुआ। उन्होंने संस्कृत साहित्य का अध्ययन जारी रखा और साहित्यशास्त्र पर शोध किया। ‘अलंकार साहित्य का इतिहास’ जैसे ग्रन्थ के प्रथम संस्करण पर ही उन्हें पांच सौ रुपए की नकद राशि प्राप्त हुई, जिससे उन्होंने तुरन्त उच्च न्यायालय की सनद प्राप्त कर ली।
उनका प्रिय व्यसन था शोध और अध्ययन। बाद में उन्होंने ‘धर्मशास्त्र के इतिहास’ पर कार्य किया, जो वास्तव में अद्वितीय शोथ-ग्रन्थ प्रमाणित हुआ। धर्मशास्त्र के शोधकार्य का विचार भी उनके मन में एक रोचक घटना के कारण आया। जब वह धर्मशास्त्र का अध्ययन कर रहे थे, तो इस विषय के सम्बन्ध में उन्हें पाश्चात्य विद्वानों के विचारों को भी पढ़ने का अवसर मिला। उसमें उन्होंने हर स्थान पर पाया कि पश्चिम के अधिकतर विद्वानों ने न केवल संस्कृत साहित्य के तथ्यों को तोड़ा-मरोड़ा है, बल्कि कहीं-कहीं तो धर्मशास्त्र और संस्कृत साहित्य के प्रति बहुत दुराग्रही भी हो गए। तब पांडुरंग ने अपना कर्तव्य समझा कि संसार के सामने सही तथ्यों को लाया जाए। इस कार्य के लिए उन्होंने जर्मन और फ्रांसीसी भाषाओं को भी खूबी के साथ सीखा। इसके बाद संसार के आगे धर्मशास्त्र के सम्बन्ध में सही तथ्यों को प्रस्तुत किया और पश्चिम की आंखों पर पड़े झूठे प्रचार के पर्दे को अपने पैने तर्कों से हटा दिया।
वकालत में भी पांडुरंग किसी से पीछे नहीं रहे। प्रत्येक मुकदमे में अपने पक्ष को सशक्त बनाने के लिए वह बहुत गहरा अध्ययन करते थे। अपने साथी वकीलों से, चाहे वह उनसे पद में छोटा ही क्यों न हो, बहुत ही अपनेपन का सम्बन्ध रखते थे। बार में उनकी उपस्थिति हमेशा ही आनन्दपूर्ण हुआ करती थी।
न्यायाधीश के आगे भी उनका प्रत्येक तर्क ठोस आधार लिए होता था और उनकी बहस से न्यायालय में सम्मान और गौरव का वातावरण वन जाता था। एक बार किसी न्यायाधीश ने पांडुरंग वामन काणे के किसी तर्क को ऊलजलूल (एबसर्ड) कह दिया। उन्होंने तुरन्त उत्तर दाग़ दिया, “मेरा यह तर्क तत्कालीन देश के सर्वोच्च न्यायालय प्रिवी कौंसिल की न्याय सम्बन्धी समिति द्वारा प्रदान किए गए निर्णय पर ही आधारित है श्रीमान !” साथ ही उस निर्णय की प्रतिलिपि उन्होंने न्यायालय को दिखाई। न्यायाधीश चुप हो गए और उनके पास काणे के पक्ष में निर्णय देने के अलावा दूसरा विकल्प ही नहीं बचा।
जहां तक हिन्दू क़ानून का सम्बन्ध है, पांडुरंग वामन काणे का कथन या मत अन्तिम और अधिकृत समझा जाता था। 1933 में सरकार ने पूना स्थित डेकन कॉलेज बन्द कर देने का निर्णय ले लिया। हालांकि पांडुरंग उसके पूर्व छात्र नहीं थे, फिर भी मन में उस कॉलेज के प्रति अपार सम्मान था, क्योंकि वहां से तिलक और आंग्रेकर जैसी महान हस्तियां पढ़कर निकली थीं। कॉलेज एक ट्रस्ट द्वारा चलाया जाता था। इसलिए उसे बन्द करने का अधिकार सरकार को था ही नहीं।
पांडुरंग वामन काणे कॉलेज के सभी पूर्व छात्रों से मिले और एक संगठन बनाया। बी. जी. खेर, जो बाद में बम्बई प्रान्त के शिक्षा मन्त्री और फिर मुख्यमन्त्री भी हुए, उस समय बम्बई में सालिसिटर का कार्य करते थे। उन्होंने इस सम्बन्ध में सहायता दी। डॉ. एन. आर. जयकर ने भी मदद की। सबने एक साथ मिलकर न्यायालय में सरकार के विरुद्ध मुक़दमा चलाया। पूना के न्यायाधीश ने कॉलेज बन्द करने पर रोक लगा दी। सरकार ने बम्बई के उच्च न्यायालय में अपील दायर कर दी। सुनवाई शुरू हुई और उच्च न्यायालय ने भी पूना के जिला न्यायालय के निर्णय को ही माना।
पांडुरंग वामन काणे समाज सुधारक भी थे। समाज में प्रचलित ढकोसलों, रूढ़ियों और कुरीतियों को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते थे। जब वह बम्बई की ब्राह्मण सभा के सभापति थे, तब गणपति उत्सव में भाग लेने के लिए हरिजनों को भी अनुमति दे दी। पांडुरंग की इस उदारता से कुछ कट्टरपन्थी बौखला उठे। उन्होंने कोर्ट में मुक़दमा चला दिया। इस केस में कट्टरपन्थियों के वकील मोहम्मद अली जिन्ना थे । पांडुरंग अपने शास्त्र सम्मत और अकाट्य तर्कों से जीत गए। हरिजनों को गणपति उत्सव में शामिल होने की अनुमति मिल गई। ब्राह्मण सभा की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए भी उन्होंने जी-जान से प्रयत्न किया और घर-घर जाकर धन इकट्ठा किया।
बम्बई के मराठी ग्रन्थ संग्रहालय से भी पांडुरंग वामन काणे का घनिष्ठ सम्बन्ध रहा और उसके लिए उन्होंने धन इकट्ठा किया। इसके भवन के लिए भी प्रयत्नशील रहे । संग्रहालय के तो वह आजीवन सदस्य थे। वह विनायक मंडल के भी वर्षों तक अध्यक्ष रहे।
पांडुरंग वामन काणे ने एक अवसर पर गोद प्रथा के क़ानून के सम्बन्ध में सुझाव दिया था कि गोद लेने वाले और गोद लिए जाने वाले पुत्र की आयु में पर्याप्त अन्तर होना चाहिए। उन्हें भय था कि इस प्रथा की आड़ में कानून का सहारा लेकर कुछ लोग अनुचित लाभ उठा सकते हैं। यदि कोई पच्चीस वर्षीय युवक किसी अठारह वर्षीय युवती को अपनी पुत्री बना लेता है, तो परिणाम अच्छे निकलने की आशा कम रहेगी।
कड़े परिश्रम में विश्वास रखने वाले पांडुरंग ने सदा ही कर्म को महत्त्व दिया। कर्म उनके लिए पूजा थी। न्यायाधीश रानाडे की तरह अपने जीवन का एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गंवाया। वह प्रतिदिन अठारह घंटे काम किया करते थे। जब कोई उनसे बात करता, तो ऋग्वेद की ऋचाओं से सजी उनकी भाषा को सुनकर तृप्त होकर लौटता। सभी लोग उन्हें प्रेम से अन्ना साहेब पुकारते थे। पांडुरंग वामन काणे विलक्षण बुद्धि और अपार ज्ञान के भंडार थे। कार्ल मार्क्स हो या कौटिल्य या कीट्स, नारद हो, चाहे न्यूटन, उनका सभी पर समान अधिकार था। वह बात-बात पर वशिष्ठ या वाल्मीकि का उदाहरण दिया करते।
अपने स्वाभिमान के चलते उन्होंने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, चाहे वह व्यक्ति हो, चाहे सरकार। तब के मुख्यमन्त्री यशवन्त राव चव्हाण ने एक बार कहीं ज़िक्र किया था कि उनसे पांडुरंग का कभी भी सम्पर्क नहीं हुआ। उन्होंने सरकार से कभी भी कुछ नहीं चाहा। शायद वह बम्बई विश्वविद्यालय के पहले और अन्तिम उपकुलपति थे, जो अपने घर से कार्यालय ट्राम में आते-जाते थे। सरकारी निमन्त्रणों पर भी जाते, तो किराए की गाड़ी में।
अठारह पुस्तकों, पांच मराठी ग्रन्थों के अतिरिक्त ढेर सारा लेखन करने वाले पांडुरंग वामन काणे ने भरपूर आनन्द और पवित्रता के साथ जीवन जिया। वह वास्तव में भारतीय संस्कृति के दिव्य दूत थे, जिन्होंने अपने ज्ञान के प्रकाश से सारे संसार को जगमगाया। अकेले 6 हज़ार पृष्ठों के महान ग्रंथ ‘धर्मशास्त्र का इतिहास’ ने उनकी ख्याति को सारी दुनिया में पहुंचाया।
भारतीय चिंतन, धर्म और अध्यात्म पर हुए कार्यों में अनेक ऐसे मनीषियों का योगदान हैं, जिन्होंने इतिहास रचा। उनमें पांडुरंग वामन काणे का नाम अग्रणी है। काणे न केवल संस्कृत और प्राच्य विद्याओं के विशारद, बल्कि विधिज्ञ भी थे। काणे संस्कृत के आचार्य, मुंबई विश्वविद्यालय के कुलपति तथा सन 1953 से 1959 तक राज्यसभा के मनोनीत सदस्य रहे। उन्होंने पेरिस, इस्तांबुल तथा कैंब्रिज के प्राच्यविज्ञ सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। साहित्य अकादेमी ने 1956 में उन्हें ‘धर्मशास्त्र का इतिहास’ के लिए अकादेमी पुरस्कार दिया।
काणे ने अपने विद्यार्थी जीवन के दौरान संस्कृत में नैपुण्य तथा विशेषता के लिए सात स्वर्ण पदक प्राप्त किए और संस्कृत में एमएस की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके बाद बंबई विश्वविद्यालय से एलएलएम की उपाधि प्राप्त की। इसी विश्वविद्यालय ने आगे चल कर उन्हें साहित्य में डीलिट की उपाधि दी। भारत सरकार की ओर से उन्हें महामहोपाध्याय की उपाधि से विभूषित किया गया।
सन् 1947 में उन्हें बम्बई विश्वविद्यालय का उपकुलपति भी नियुक्त किया गया था। सन् 1948 में पेरिस से बुलाई गई प्राच्य विद्या परिषद में डॉ. राधाकृष्णन् के नेतृत्व में डॉ. काणे ने भाग लिया था। इसी परिषद के निमन्त्रण पर वह इस्ताम्बूल और कैम्ब्रिज भी गए। 1953 से 1958 तक और उसके बाद भी वह राज्यसभा के सदस्य रहे। 1959 में भारतीय प्राच्य विद्या के राष्ट्रीय अध्यापक भी रहे।
उनकी असीम विद्वत्ता और समाज-सेवा को ध्यान में रखकर ही भारत सरकार ने उन्हें 1963 में भारतरत्न की सर्वोच्च उपाधि से सम्मानित किया। 18 अप्रैल 1972 को 92 वर्ष की अवस्था में पांडुरंग वामन काणे ने अपने शरीर को त्याग दिया। लेकिन जो अनमोल ज्ञान वे छोड़ गए हैं, उसका महत्त्व अपरिमित है। विद्वानों की दुनिया उन्हें भुला नहीं सकती। उनकी कल्पना तार्किक थी। उन्होंने लिखा है, ‘भारतीय संविधान भारतीय संस्कृति के अनुरूप नहीं है, क्योंकि लोगों को अधिकार तो दिए गए हैं, लेकिन जिम्मेदारी नहीं दी गई।’ आज कौन उनकी इस बात से इनकार करेगा? भारत में लोगों को हर संभव अधिकार मिले हुए हैं, लेकिन लोग जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं हैं, जिससे समाज में अनेक चुनौतियां खड़ी हो गई हैं।
 Narvilnews Whole world at one eyesight
Narvilnews Whole world at one eyesight