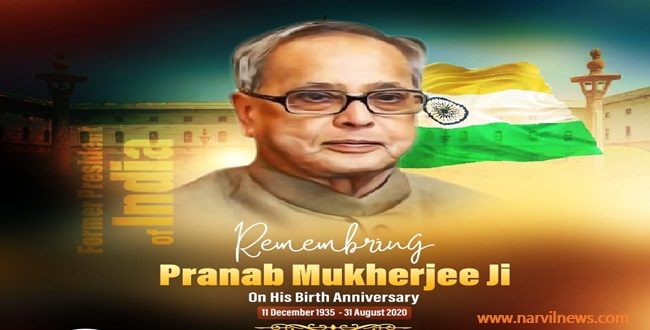डॉ. भगवान दास, भारत रत्न- 1955
(जन्म- १२ जनवरी १८६९, मृत्यु- १८ सितम्बर १९५८)
काशी ने देश को कई रत्न दिए। उन्हीं में से एक रत्न डा. भगवान दास का भी नाम शामिल है। डा. भगवान दास जीवनपर्यंत चिंतन, मनन, लेखन करते रहे। “हमारे देश में अनेक जातियों और धर्मों के लोग रहते हैं, परन्तु इन सभी में भिन्नता होने के साथ-साथ सभी जातियां और धर्म एक ही रंग में रंगे हैं। उन सबकी संस्कृति एक-सी ही है, क्योंकि वे हमारे उस देश की माटी में फले-फूले हैं, जिस माटी से मानवता की खुशबू आती है। यहां पर सभी धर्मों का निवास मानवता में है।”
इस प्रकार की विचारधारा के उपासक डॉ. भगवान दास का जन्म 12 फ़रवरी 1869 को, वाराणसी के एक वैश्य परिवार में हुआ था। पिता साह माधवदास की गणना बनारस के सम्मानित व्यक्तियों में होती थी। उनके पूर्वज साह मनोहरदास कलकत्ता के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे।
डॉ. भगवान दास के पिता ने नागरी प्रचारणी सभा, कार्निकल लाइब्रेरी तथा सेंट्रल हिन्दू कॉलेज की स्थापना में भी हर प्रकार का सहयोग दिया था । वह सभी धर्मों को समान मानने वाले उदार व्यक्ति थे। जहां उनके मित्र सर सैयद अहमद खां थे, वहीं दूसरी ओर महर्षि दयानन्द सरस्वती भी उनके अच्छे मित्र थे । माधवदास हरेक वर्ग के लोगों में लोकप्रिय थे और उनका बड़ा सम्मान किया जाता था। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, महाराजा कश्मीर, दीनबन्धु सी.एफ. ऐंडूज़, फ्रांसीसी लेखक मोनशायर शेवरलिन, जापान के विद्वान एकाई काबागूची, चीन के साहित्यकार लिन यु तांग उनके बहुत अच्छे मित्र थे।
भगवान दास को अपने पूर्वजों से विरासत में व्यापार मिला था । उनका परिवार सोलहवीं शताब्दी में हरियाणा के अग्रोहा से दिल्ली आया था, फिर हुमायूं की फ़ौज के साथ पूर्वी उत्तर-प्रदेश में मिर्ज़ापुर ज़िले के चुनार और आहरुरा नामक क़स्बों में बस गया था। बाद में उनके पुरखे बनारस जाकर बस गए और अठारहवीं शताब्दी में कुशल व्यापारी के रूप में प्रसिद्ध ईस्ट इंडिया कम्पनी से उनके अच्छे व्यापारिक सम्बन्ध हो गए। इससे उनका व्यापार सूरत, बम्बई, मद्रास और मछलीपटनम तक फैल गया। अंग्रेज़ों के भी ये लोग साहूकार थे और मछलीपटनम में उनकी अपनी टकसाल तक थी। मैसूर के टीपू सुल्तान के विरुद्ध अंग्रेज़ों के साथ श्रीरंगापटनम का युद्ध भी उन्होंने लड़ा था। इस युद्ध में नाम के साथ-साथ दौलत भी अर्जित की, क्योंकि पूरी रसद का ठेका उनके परिवार के पास था। इसके बाद ही कलकत्ता में एक बड़ा बाज़ार बनवाया। आज भी वहां की मनोहरदास स्ट्रीट उनके परिवार की याद दिलाती है। कलकत्ता का मैदान, जो अब विधानचन्द्र मैदान कहलाता है, भगवान दास के पूर्वजों द्वारा दान में दिया गया एक नमूना है।
ऐसे परिवार में डॉ. भगवान दास का जन्म हुआ था, जिनके गुणों को गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने भी सराहा था। गुरुदेव ने एक सज्जन से कहा था, “आप मेरे पास दर्शन से सम्बन्धित यह प्रश्न क्यों पूछने आए हैं, जब कि भगवान दास जैसे दार्शनिक, बुद्धिमान और योग्य पुरुष विद्यमान हैं।” सच्चाई यही है कि डॉ. भगवान दास को राजनेता की अपेक्षा दर्शनशास्त्री के रूप में ज़्यादा जाना जाता है की डॉ. भगवान दास बाल्यकाल से ही प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने बारह वर्ष आयु में मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली थी। उन दिनों फारसी और उर्दू पढ़ने और बोलने का रिवाज़ था। समय को देखते हुए बालक भगवान दास को भी फ़ारसी और उर्दू की शिक्षा दी गई और छोटी-सी आयु में उन्होंने शेख सादी के ‘गुलिस्तां’, ‘बोस्तां’ पर महारत हासिल कर अपनी तेज़ बुद्धि का परिचय दिया। परिवार और शहर बनारस के माहौल को देखते हुए उन्हें संस्कृत भी पढ़ाई गई। जब कि रीति के अनुसार उन दिनों संस्कृत केवल ब्राह्मणों को ही पढ़ाई जाती थी।
एफ.ए. (इंटरमीडिएट) में उनके विषय थे – नागरिकशास्त्र, अंग्रेज़ी, संस्कृत, मनोविज्ञान, तर्कशास्त्र, गणित और इतिहास। उस समय तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय शुरू नहीं हुआ था और बनारस का क्वीन्स कॉलेज कलकत्ता विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ था। भगवान दास ने अठारह वर्ष की आयु में कलकत्ता विश्वविद्यालय से दर्शनशास्त्र में एम.ए. की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। एंट्रेंस से एम. ए. तक वह सदा विशेष योग्यता के साथ परीक्षाएं पास करते रहे।
इसी बीच उन्होंने हिन्दी, अंग्रेज़ी, संस्कृत, अरबी और फ़ारसी भाषाओं का बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया । इक्कीस वर्ष की उम्र में ही डॉ. भगवान दास उत्तर-प्रदेश में तहसीलदार बन गए। बाद में डिप्टी कलक्टर और मजिस्ट्रेट भी रहे। ग़ाज़ीपुर, कंचनपुर व इलाहाबाद की तहसीलों में तहसीलदारी करने के पश्चात वह आगरा और बाराबंकी में डिप्टी कलक्टर रहे।
डॉ. भगवान दास का मन सरकारी नौकरी से प्रसन्न नहीं था। उन्होंने शुरू में केवल आठ वर्ष ही सरकारी नौकरी की, वह भी पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए। 1897 में उनके पिता का देहान्त हो गया। इसके बाद उन्होंने अपनी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। उसी समय वह वाराणसी में एक कॉलेज की स्थापना में जुट गए। आख़िर वहां सेंट्रल हिन्दू कॉलेज की नींव पड़ी। अंग्रेज़ सरकार ने इस कॉलेज के लिए अनुदान देने से साफ़ इनकार कर दिया, क्योंकि कॉलेज में धर्म की शिक्षा अनिवार्य थी। धन की कमी के कारण कॉलेज को चलाने में कठिनाई होने लगी, तो उत्साही युवक धन एकत्र करने में जुट गए।
डॉ. भगवान दास और उनके भाई गोविन्ददास विभिन्न रियासतों के राजा-महाराजाओं के पास गए और उनसे दान इकट्ठा करके कॉलेज के काम को आगे बढ़ाया। इतना ही नहीं, उन्होंने इस कॉलेज में साहित्य और दर्शनशास्त्र पढ़ाने की ज़िम्मेदारी भी अपने ऊपर ले ली और उसे पूरी सफलता के साथ निभाया।
जब भगवान दास इलाहाबाद में तहसीलदार थे, उनका परिचय थियोसोफिकल आन्दोलन की सक्रिय नेता डॉक्टर एनी बेसेंट से हुआ। थियोसोफी के मतानुसार आध्यात्मिक विचारधारा का मूल स्रोत भारत है। एनी बेसेंट से भगवान दास बहुत प्रभावित हुए और थियोसोफिकल आन्दोलन में सक्रियता से भाग लेने लगे। उन्हीं के साथ भगवान दास ने भारत भ्रमण भी किया। उनका मत था कि बच्चों को धर्म की शिक्षा अवश्य देनी चाहिए। डॉ. भगवान दास की मेहनत का ही फल था कि थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्य कार्यालय मद्रास से बनारस पहुंच गया और एनी बेसेंट भी बनारस में रहने लगीं। यहां उनके ही सहयोग से सेंट्रल हिन्दू कॉलेज की स्थापना हो सकी थी। उन दिनों ढेरों बुद्धिजीवी थियोसोफिकल आन्दोलन से प्रभावित हो चुके थे|
कॉलेज में साहित्य और दर्शनशास्त्र को पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा था कि छात्र मुग्ध हो जाते थे। इन्हीं दिनों उनकी मुलाक़ात पंडित मदन मोहन मालवीय से हुई और उन्होंने हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना में अपना सारा श्रम लगा दिया। वह स्वयं कसरती बदन वाले पुरुष थे। रोज़ाना डंड-बैठक लगाते और गदा व मुगदर भांजते थे। अपनी घोड़ागाड़ी स्वयं ही चलाते थे। ये आदतें काफ़ी उम्र तक उनके साथ रहीं। मिलनसार मिजाज़ का मालिक होने के कारण सभी उनसे मिलने और उनके ज्ञान से भरपूर लाभ उठाने के लिए उत्सुक रहते थे। उनका निशाना अच्छा और सधा हुआ होने के बावजूद वह शिकार नहीं खेलते थे। उन्हें संगीत पसन्द था और सितार पर भक्ति गीत सुनने का बहुत शौक़ था। इसके अलावा कव्वाली भी पसन्द थी । विचारों के मामले में भगवान दास को पुरातनी ही कहा जा सकता है, पर वह कट्टरपन्थी नहीं थे। वह वर्ण व्यवस्था में विश्वास रखते थे और उनका विश्वास था कि मानवता के कल्याण तथा स्थिरता के लिए ‘मनुस्मृति’ में जो चार वर्ण बताए गए, ठीक उसी प्रकार मानव जीवन को चार आश्रमों में बांटा गया है।
सन् 1920-21 में जब सारे देश में असहयोग आन्दोलन अपने चरम पर था, तब वह भी उस आन्दोलन में कूद पड़े और उन्हें जेल जाना पड़ा। उन दिनों ऐसे शिक्षा केन्द्रों की ज़रूरत थी, जिनसे छात्रों के मन में देशहित की भावना पैदा की जा सके। इसलिए काशी में ऐसी ही एक संस्था काशी विद्यापीठ की स्थापना की गई। इस विद्यापीठ में पढ़ाने वालों में डॉ. सम्पूर्णानन्द, आचार्य नरेन्द्रदेव, आचार्य कृपलानी तथा स्वयं डॉ. भगवान दास जैसी विभूतियां थीं।
डॉ. भगवान दास के संयम से भरे जीवन, कर्म के प्रति निष्ठा और उदारता का छात्रों पर गहरा प्रभाव पड़ा। वह मानवता के पुजारी थे। सभी धर्मों में उनकी समान आस्था थी। उनमें राष्ट्र-प्रेम की भावना कूट-कूटकर भरी हुई थी। भूतपूर्व प्रधानमन्त्री लालबहादुर शास्त्री उनके ही शिष्य थे। डॉ. साहब की याददाश्त इतनी तेज़ थी कि संस्कृत के सैकड़ों श्लोक ज़बानी याद थे । बाद में वह काशी विद्यापीठ के प्रथम कुलपति बना दिए गए।
वह राजनीति में भी भाग लेते थे, फिर भी उनका वास्तविक क्षेत्र दर्शन एवं शिक्षा ही रहा। उनके राजनीतिक लेखों में भी दर्शन और अध्यात्म झलकता था। वह यह साबित करना चाहते थे कि भारत के लोग आरम्भ से ही स्वतन्त्रता- प्रेमी हैं । स्वतन्त्रता की ललक या यह विचारधारा उनकी अपनी थी। वह कहते थे कि आज़ादी का अर्थ आत्मा की स्वतन्त्रता से है, जो विदेशी सत्ता के कारण बंधी हुई है। आज का बहुचर्चित शब्द कॉमनवेल्थ सबसे पहले डॉ. एनी बेसेंट के ही मुख से निकला था, जिसका समर्थन डॉ. साहब ने किया था।
सर्वधर्म समभाव और मानव जाति की एकता का प्रयास उनके लिए केवल कथनी ही नहीं, बल्कि उनके दैनिक व्यवहार के अंग भी थे। 1931 में जब काशी और कानपुर में दंगे हुए, तब भगवान दास का कबीर जैसा पवित्र हृदय फूट-फूटकर रो पड़ा। सन् 1932 में पूना की यरवदा जेल से गांधी जी ने भगवान दास को एक महत्त्वपूर्ण ज़िम्मेदारी सौंपी कि वह सिद्ध करें कि हरिजनों का मन्दिरों में प्रवेश कोई धार्मिक हानि नहीं है। उन्होंने इस ज़िम्मेदारी का भली-भांति निर्वाह किया था।
हालांकि डॉ. भगवान दास के सम्बन्ध अंग्रेज़ अधिकारियों से हमेशा मधुर रहे, परन्तु उन्होंने उनके साथ विचार करते समय अपने देश के पलड़े को कभी हलका नहीं होने दिया। वह हिन्दू-मुस्लिम एकता के सदा तरफ़दार रहे। जब कभी कहीं दंगा हो जाता, तो वह अपनी जान हथेली पर रखकर वहां जा पहुंचते और शान्ति स्थापित करते। देश के बंटवारे ने भी उन्हें बेहद पीड़ा पहुंचाई थी।
हिन्दी साहित्य से उन्हें गहरा प्यार था। हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग और नागरी प्रचारिणी सभा से उनका निकट सम्बन्ध रहा। सन् 1921 में कलकत्ता में आयोजित हिन्दी साहित्य सम्मेलन के वह सभापति बनाए गए थे। अपनी लिखी हुई पुस्तकों में वह ‘एशेंसियल यूनिटी ऑफ़ ऑल रिलीजंस’ को सबसे पहला स्थान देते थे । इस पुस्तक का हिन्दी रूपान्तर पंडित सुन्दरलाल ने किया था, जिसका नाम है, ‘सर्वधर्मों की बुनियादी एकता’। इसके अलावा ‘दर्शन का प्रयोजन’ एवं ‘पुरुषार्थ’ नामक दोनों पुस्तकें उन दिनों बड़ी लोकप्रिय हुईं। तीस वर्ष की आयु में पहली पुस्तक ‘भावनाओं का विज्ञान’ (साइंस ऑफ़ इमोशंस) प्रकाशित हुई। अंग्रेज़ी में विशेष दक्षता के कारण उन्होंने अधिकतर अंग्रेज़ी में ही लिखा, जिससे भारत ही नहीं, विदेशों का भी ध्यान भी उनकी ओर गया। मित्रों के आग्रह पर कई पुस्तकें हिन्दी में भी लिखीं|
हर वस्तु को ढंग से रखने का उन्हें विशेष चाव था। उनकी आलमारियों में पुस्तकें लगी रहती थीं, जिनमें से लगभग सभी पढ़ चुके थे। पुस्तकें पढ़ना और उन्हें सुन्दर हस्तलिपि में साफ़-साफ़ नोट करना उनकी रुचि थी। यदि किसी पुस्तक में उन्हें व्याकरण सम्बन्धी अशुद्धि मिल जाती, तो तुरन्त ठीक कर देते। उन्होंने पुस्तकों के हाशियों पर कभी कुछ नहीं लिखा। उनकी सारी पुस्तकें इतनी अच्छी हालत में रहतीं कि लगता, जैसे नई हों। अपनी मृत्यु से पूर्व उन्होंने सारी पुस्तकें हिन्दू विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ को दान में दे दी थीं।
वह बहुत व्यावहारिक थे। उनका कहना था, “इसमें सन्देह नहीं कि मैं वेदान्त दर्शन को मानता हूं, पर इसका यह मतलब भी नहीं कि आप मेरी जीभ पर पिसी हुई तेज़ और तीखी मिर्चें रख दें और मुझे उसका तीखापन महसूस न हो।” वह अधिकतर गम्भीर ही रहते थे, परन्तु टंडन जी के साथ उनका मज़ाक़ चलता रहता था। इसकी छूट सिर्फ़ टंडन जी को ही थी । बहुत-से अंग्रेज़ कमिश्नर उनके निवास स्थान पर उनसे मिलने आते थे। प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन के बहिष्कार के सम्बन्ध में जिन अंग्रेज़ अधिकारियों ने उन्हें एक वर्ष का कारावास दिया था, वह भी उनसे मिलने आते थे। इतना सम्मान था उनका |
जब वह म्युनिसिपल बोर्ड के अध्यक्ष थे, उन्हें कमिश्नर का पत्र प्राप्त हुआ । पत्र की भाषा थोड़ी फूहड़ थी। भगवान दास ने पत्र की मूल प्रति पर ही यह लिखकर उसे वापस कर दिया कि उचित भाषा न होने के कारण मूल पत्र वापस किया जाता है। पत्र वापस पाकर दूसरे दिन कमिश्नर स्वयं भगवान दास के पास आए और उस स्थिति के लिए शर्मिन्दगी प्रकट की।
वह प्रशासन में बहुत कुशल और तीव्र थे। बड़े-से-बड़े और पेचीदा कार्यों को भी वह तुरन्त निपटा देते थे। उनकी हस्तलिपि बहुत सुन्दर थी और अधिकतर फ़ाइलों पर टिप्पणियां स्वयं लिखते थे। बोर्ड की अध्यक्षता के काल में उन्होंने ‘श्रीमद्भगवद्गीता’ का अनुवाद भी किया था, जिसमें एनी बेसेंट का भी बड़ा सहयोग रहा।
विचारों और साहित्यिक सेवाओं से प्रभावित होकर काशी हिन्दू विश्वविद्यालय एवं इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने उन्हें डॉक्ट्रेट की मानद उपाधियां प्रदान कीं। देश-भक्ति, विद्वत्ता, शिक्षा और साहित्य में योगदान के लिए भारत सरकार ने 1955 में उन्हें भारतरत्न की सर्वोच्च उपाधि से विभूषित किया। 1958 में उनकी पुस्तक ‘विविधार्थ’ प्रकाशित हुई । सम्भवतः यह उनकी अन्तिम रचना थी, क्योंकि महानता का वह सूर्य 90 वर्ष की आयु में 18 सितम्बर 1958 को, रात आठ बजे अस्त हो गया।
 Narvilnews Whole world at one eyesight
Narvilnews Whole world at one eyesight