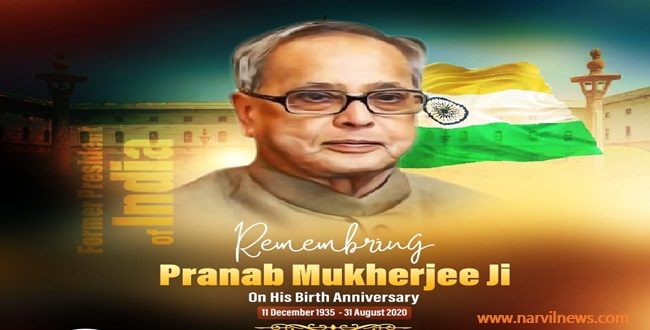डॉ. धोन्धू केशव कर्वे (भारतरत्न- 1958)
(जन्म-18 एप्रिल 1858, मृत्यु- 9 नोव्हेंबर 1962)
“सब इंसान बराबर हैं। न कोई छोटा है, न बड़ा। हम आज़ादी के बाद भी दुर्बल हैं, दरिद्र हैं और नैतिक रूप से कमज़ोर हैं, क्योंकि हमारे उद्देश्यों, विचारों और कर्मों में समता और ममता का स्थान नहीं रहा। हमें नैतिक रूप से मज़बूत बनने के लिए अपने विचारों और कर्मों में समता को जगाना होगा।” ये महान विचार हैं समाजसेवी डॉ. घोन्धूकेशव कर्वे के, जिन्हें सम्मान के साथ अण्णा साहब कहा जाने लगा।
वह ज़माना पेशवाओं का था। पेशवाओं की राजधानी पुणे में कोंकण से दो भाई केशव भटकर्वे और रघुनाथ भटकर्वे आए। उन्होंने वहां एक दुकान खोली। थोड़े समय में ही उनका व्यापार अच्छा चल निकला।
उनकी व्यापारिक उपलब्धि यह थी कि पेशवा स्वयं उनकी दुकान से सौदा मंगवाने लगे। बड़े भाई केशव भटकर्वे की विद्वत्ता के कारण पेशवा उनसे खुश हो गए और एक गांव हतनोर की जागीर उन्हें भेंट में दे दी। केशव भटकर्वे अग्निहोत्री ब्राह्मण थे। अतः पेशवाओं के धार्मिक कार्यकलापों में भी उपस्थित रहते थे।
छोटे भाई रघुनाथ व्यापार को दिन दूना रात चौगुना बढ़ाते रहे। अपने बड़े भाई की वह इतनी इज़्ज़त करते थे कि सारा व्यापार उन्हीं के नाम से चलाते। बढ़िया व्यापार के कारण धन-धान्य की कोई कमी नहीं थी। ज़रूरत पड़ने पर मराठा सरदारों को ऋण भी देते थे। एक बार दासजी गायकवाड़ ने उनसे साढ़े छह लाख रुपए उधार लिए थे। नागपुर के भोंसले भी उनके ऋणी थे।
वही दासजी गायकवाड़ बड़ौदा के शासक बने। उनके वंशज महाराज गायकवाड़ एक दिन कर्वे के गांव मुरद में आकर ब्राह्मणों को दान-दक्षिणा दे रहे थे। हरेक ब्राह्मण को दस रुपए मिल रहे थे। भीखू और धोन्धू दोनों भाइयों को भी यह पता चला। वे दक्षिणा लेने के लिए अपनी मां की आज्ञा लेने घर की ओर दौड़े। मां ने कहा कि वह दक्षिणा नहीं, भीख है और हम इतने गिरे हुए नहीं कि भीख लेने जाएं, पर धोन्यू ज़िद करता रहा और उसे दक्षिणा कहता रहा। बड़ौदा के महाराज दक्षिणा दे रहे हैं, इसे वह बहुत बड़ी बात मानता रहा। मां ने कहा कि हम उनसे कम नहीं। वह भी हमारे क़र्ज़दार हैं। हमारे पुरखों ने उनके पुरखों को छः लाख दिए थे, जिसे आज तक वे उतार नहीं पाए।
मां की बात सुनकर नन्हा धोन्धू आश्चर्य से भर उठा। 18 अप्रैल,1858 को, महाराष्ट्र के रत्नागिरि जिले के एक गांव में जन्मा धोन्धू, उन्हीं केशव और रघुनाथ भटकर्वे की भावी पीढ़ी था, धोन्धू के पिता केशव पन्त ने, बचपन में ख़ूब अमीरी भोगी थी, परन्तु धीरे-धीरे घर की धन-सम्पत्ति चुकने लगी। उनकी स्वाभिमानी पत्नी लक्ष्मीबाई दुर्भाग्य के ये दिन पहले ही भांप गई।
केशव पन्त तो घर से बाहर रहते थे, लक्ष्मीबाई ने बहुत होशियारी से थोड़ा-थोड़ा करके धन बचाया और ज़मीन ख़रीदकर घर बनाया। परिवार पर जो कर्जा था, उसे भी चुकाया। इसी बीच उनके छः बच्चे हुए। पहले तीन बच्चे बचे नहीं। दु:ख तथा परेशानी को सहते हुए भीखू, धोन्धू और उनकी छोटी बहन अम्बा को उन्होंने पाला-पोसा।
ज़िद्दी धोन्यू डरपोक भी थे। समुद्र के पास रहते हुए भी उन्होंने कभी तैरने की हिम्मत नहीं की। एक बार साथियों ने उन्हें ज़बर्दस्ती हाथ-पांव बांधकर पानी में डाल दिया। धोन्धू ने बड़ा शोर मचाया और चिल्ला-चिल्लाकर राहगीरों को इकट्ठा कर लिया। उनके मन में ऐसा डर समाया कि घर आकर अंधेरी अटारी में छिप गए। किसे पता था कि आगे चलकर यही ज़िद्दी और डरपोक बालक बहादुरी के साथ समाज में फैली रूढ़ियों का डटकर मुकाबला करेगा और समाज की भलाई के अनेक काम करके महर्षि का पद प्राप्त करेगा।
हाथ में तख्ती लेकर वह शेनवी पन्तोजी की प्राइमरी पाठशाला में जाने लगे। वहां बांस की क़लम से लिखना सीखा। कितने ही पुराने श्लोकों को कंठस्थ कर लिया, जिन्हें वह मधुरता से गाकर सुनाते थे। इस प्राइवेट स्कूल से चौथी कक्षा तक पढ़ाई की। बाद में सोमण गुरुजी द्वारा संचालित सरकारी विद्यालय में छठी तक पढ़े । यह विद्यालय मुरद से छः मील दूर दपोली में था
उन्हें गणित से विशेष लगाव था। शिक्षा के साथ वह रोज़ राम विजय, हरि विजय, शिव लीला, अमृत, गुरु चरित्र का पाठ करते। जब कभी धार्मिक उत्सव का समापन समारोह होता, तो धोन्धू से श्लोक पाठ करने को कहा जाता। दुर्गा देवी मन्दिर में उन्होंने अपने एक अध्यापक के सहयोग से वाचनालय शुरू किया। अध्यापक के एक मित्र पांडुरंग कई समाचार-पत्र मंगाते थे। वही वाचनालय में रख दिए जाते थे। धोन्धू बड़ी लगन से वाचनालय में काम करते।
समाज-सेवा का बीज धोन्धू के मन में इस वाचनालय से ही पड़ा। आगे चलकर उन्हीं अध्यापक के सहयोग से उन्होंने सहकारी भंडार खोला। पांच-पांच रुपयों के शेयर बेचे और पूंजी 800 रुपए तक की गई, परन्तु हिसाब-किताब ठीक से न रख पाने के कारण भंडार चल नहीं पाया। बड़ी मुश्किल से भागीदारों को उनका पैसा चुका पाए। कुछ लोगों ने उन्हें माफ़ भी कर दिया।
उन दिनों छठी कक्षा की परीक्षा बम्बई, रत्नागिरी और सतारा में हुआ करती थी। 1875 का सितम्बर महीना था। वर्षा मूसलाधार चल रही थी। छठी कक्षा की परीक्षा देने वे अपने चार अन्य साथियों के साथ सतारा जाने के लिए निकल पड़े। दिन-रात पैदल चले। रास्ते की गहरी घाटी और पर्वत की चोटी के बीच पड़ने वाले कंटीले रास्तों को पार करके जब वह प्रवेश समिति के अध्यक्ष के सामने पहुंचे, तो उसने देखते ही उनसे उनकी उम्र पूछी। उन्होंने सत्रह वर्ष बताई, पर अध्यक्ष ने उसे नहीं माना और उन्हें पन्द्रह वर्ष का ही बताते रहे। इसलिए उनका प्रवेश न हो सका और निराश होकर उन्हें लौटना पड़ा।
बाद में वह अपने भाई के साथ कोल्हापुर से परीक्षा पास कर पाए। दो वर्ष बाद उन्हें पढ़ने के लिए रत्नागिरि या बम्बई जाना आवश्यक हो गया। उनके पिता पढ़ाई का खर्च उठाने में स्वयं को मजबूर पा रहे थे। धोन्धू के उत्साह को देखकर उन्होंने किसी-न-किसी तरह धन की व्यवस्था की और उन्हें रत्नागिरि भेज दिया।
उन दिनों अंग्रेज़ी भाषा का काफ़ी महत्त्व था । उसी के सहारे तरक़्क़ी कर पाना आसान था । रत्नागिरि के हाईस्कूल में प्रवेश लेने का यह भी एक कारण था, परन्तु स्वास्थ्य ने उनका साथ नहीं दिया। वह बीमारी के कारण गांव लौट आए और पांच रुपए प्रति माह पर अध्यापन का काम शुरू कर दिया। साथ में पढ़ाई को भी जारी रखा। सात घंटे स्कूल में पढ़ाना और फिर घर आकर अपनी अंग्रेज़ी की पढ़ाई करना। इस प्रकार कुछ धन कमाकर वह अपने एक दोस्त के साथ बम्बई के विल्सन स्कूल में भर्ती हो गए। सन् 1881 में मैट्रिक परीक्षा पास करने के बाद सन् 1884 में एल्फिस्टन कॉलेज से गणित में बी. ए. की परीक्षा पास कर ली। एल्फिस्टन कॉलेज में धोन्धू केशव कर्वे के सहपाठियों में थे, महान देशभक्त गोपालकृष्ण गोखले, गणितज्ञ चिमनलाल सीतलवाड़ और राजनीतिज्ञ वकील टी.के. गज्जर।
इस बीच उनके पिता की मृत्यु हो गई। बम्बई में वह अपनी पत्नी राधाबाई और पुत्र रघुनाथ को ले आए। परिवार के ख़र्चे के लिए उन्होंने ट्यूशन आरम्भ कर दी। राधाबाई ने भी पढ़ना शुरू किया और वह शीघ्र ही मैट्रिक की परीक्षा देने योग्य हो गई।
वामन आवाजी मोडक उन दिनों एल्फिस्टन कॉलेज के प्रधानाचार्य थे। वह धोन्धू से परिचित भी थे। धोन्यू उनके यहां कुछ दिन रत्नागिरि में ठहरे भी थे। उसी याद और परिचय के सहारे वह उनके पास अरवारी रुप से अध्यापन का कार्य मांगने पहुंचे।
कम उम्र के कारण मोड़क महाशय के मना करने पर धोन्धू केशव ने नहीं मानी और वह एल्फिस्टन कॉलेज के अपने दयालु व परिचित प्रि हैथोरुथ वाइट से मिले, जिनके प्रयास से उन्हें अस्थायी तौर पर अपरा लिया गया। इसके साथ प्रोफेसर साहब ने उन्हें प्राइवेट ट्यूशन भी दिलवा दीं। इससे उनकी ज़िन्दगी की गाड़ी के पहिए चल निकले। स्कूल में काम अच्छा रहा, तो मोडक ने उन्हें स्थायी कार्य देना चाहा। स्वाभिमानी करें ने उन्हें मना कर दिया। इसके बाद उन्होंने मेहनत करके रसायन और भौतिक विज्ञान में एम.एस-सी. किया।
उन्हीं दिनों राबर्ट मनी स्कूल के एक अध्यापक राजाराम शास्त्री भागवत ने, बम्बई में मराठा हाईस्कूल खोला और अपने प्रिय शिष्य कर्वे को अध्यापन के लिए बुला लिया। धोन्धू केशव अपने गुरु की यह आज्ञा मानकर आजीवन मराठा हाईस्कूल के हो गए।
उनकी जीवनचर्या बहुत व्यस्त हो गई। सुबह छः बजे मझगांव में सेंट पीटर्स स्कूल के भारतीय और यूरोपीय छात्रों को अंग्रेजी पढ़ाते। जिस गांव में ह रहते थे, वहां से मझगांव पैदल जाते थे। राधाबाई साढ़े चार बजे जाग जाती। पांच बजे तक दही-भात का कलेवा देकर उन्हें विदा करतीं। मझगांव में पढ़ाकर वह दिन-भर मराठा हाईस्कूल में रहते। रात में वापस आते, तो भोजन करके राधाबाई की पढ़ाई को देखते।
बेहद परिश्रम का प्रभाव पड़ा राधाबाई के स्वास्थ्य पर वह बीमार पड़ गईं। उनकी देखभाल करना कर्वे जी के बस में नहीं था। इसलिए उन्हें मुरद छोड़ आए। गांव की सुधारनिधि से वह आर्थिक रूप से छात्रों की सहायता भी किया करते थे। अपनी आय में से 5 प्रतिशत का कोप केवल सामाजिक कार्यों में दान देने के लिए ही बना रखा था। इतना ही नहीं, समाज-सेवा की भावना के कारण उन्होंने मित्रों के सहयोग से सन् 1888 में गांव में एक स्कूल की स्थापना के लिए मुरद कोष शुरू किया और उसी से एक दिन हाईस्कूल खोल लिया।
इस समाज सेवा में राधाबाई ने भी कड़ी मेहनत की, किन्तु उनका स्वास्थ्य गिरता चला गया और श्रावण की नागपंचमी के दिन राधाबाई उनका साथ छोड़कर अनन्त यात्रा पर चली गई। उन दिनों कर्वे बम्बई में थे। पत्नी का शोक मन में बसाए कार्यों में लगे रहे और अपने पसीने से कमाया गया लगभग 500 रुपए का धन उन्होंने मुरद गांव को स्त्री-शिक्षा के लिए राधाबाई स्मारक फंड के रूप में दे दिया। यही दान आधार साबित हुआ अनाथ महिला उद्धार एवं स्त्री-शिक्षा के लिए बने भव्य महिला विद्यापीठ का यह धोन्धू कर्वे का कभी न भूलाया जाने वाला महादान था।
उन्हीं दिनों पूना से गोपालकृष्ण गोखले का पत्र मिला। उन्होंने कर्वे को फर्ग्युसन कॉलेज, पूना में गणित पढ़ाने के लिए बुलावा भेजा। वह उलझन में पड़ गए। उस दिन राजाराम शास्त्री ने ही उन्हें समझाया कि अगर इस निमन्त्रण को ठुकरा दिया, तो फिर जीवन-भर इस भूल के लिए पछताना पड़ेगा।
राजाराम शास्त्री द्वारा समझाने पर वह, फर्ग्युसन कॉलेज में गणित पढ़ाने लगे। बम्बई में अध्यापन कार्य से होने वाली लगभग 300 रुपए प्रति मास की आमदनी की चिन्ता किए बिना केवल 75 रुपए मासिक पर पूना आ गए और डेकन एजुकेशन सोसाइटी के सदस्य बनकर 1914 तक शिक्षण संस्थान में सेवा करते रहे। पेंशन सहित पदमुक्त होने के बाद उनके जीवन में बदलाव आया और पूना की धरती उनकी साधना स्थली बन गई।
उन दिनों भारतीय समाज तरह-तरह की कुरीतियों में फंसा हुआ था। बाल-विवाह और सती-प्रथा जैसी कुरीतियों ने समाज को जकड़ा हुआ था। अक्सर बाल-विधवाएं यदि सती नहीं होती थीं, तो नरक भोगने को मजबूर हो जाती थीं। उनका सुबह-सुबह मुंह देखना या मांगलिक कार्यों में उनकी उपस्थिति अपशगुन मानी जाती थी। पति के मर जाने पर उनकी ज़िन्दगी बाल मुंडवाकर एक अंधेरी कोठरी में बन्द होकर रह जाती थी। विधवा पुनर्विवाह एक्ट बन गया था, परन्तु फिर भी समाज में पाखंड तब भी अपनी जड़ें जमाए हुए था।
कर्वे ने अपने मित्र की पत्नी को भी इसी प्रकार दयनीय हालत में मरते देखा, तो उन्होंने ठान लिया कि भाषणों के बल पर इस प्रथा का अन्त होना कठिन है। इसलिए उन्होंने किसी कुलीन परिवार की कन्या के साथ विवाह न करके अपने मित्र नरहर पंत की विधवा छोटी बहन गोदूबाई (गोदावरी) के साथ 13 मार्च, सन् 1893 में दूसरा विवाह कर लिया। इनका नया नाम आनंदीबाई रखा गया। इस विवाह के कारण उनके परिवारजन और समाज के लोग नाराज़ हो गए और उन्हें समाज से बहिष्कृत कर दिया गया। यहां तक कि अपने गांव में भी उन्हें रहने को स्थान नहीं दिया।
दूसरी ओर उनके इस साहसिक कदम की जागरूक जगत में सराहना की गई। ‘इन्दु प्रकाश’, ‘सुबोध पत्रिका’, ‘ज्ञान प्रकाश’, ‘सुधारक’, ‘केसरी’ और ‘वैदर्भ’ आदि प्रगतिशील समाचार-पत्रों ने उनकी प्रशंसा में अपने कॉलम रंग डाले और उन्हें बधाइयां भेजीं। बाधाओं के आने पर भी कर्वे दम्पति ने हार नहीं मानी, बल्कि दुगुनी हिम्मत से सामाजिक कुरीतियों को जड़ से समाप्त करने के लिए उनमें और भी शक्ति आ गई।
आनन्दीबाई ने राधाबाई के निधन के बाद हुए, ख़ालीपन को भर दिया। उन्होंने नागपुर के डफरिन अस्पताल से मिडवाइफ़ और नर्सिंग की शिक्षा ली। दूसरी ओर कर्वे जी ने विधवा समिति की स्थापना की। इसका उद्देश्य विधवाओं की दशा सुधारना था। उन्होंने सोचा कि महिलाओं के उद्धार के लिए विधवा विवाह ही काफ़ी नहीं है। अतः उन्होंने अनाथ बालिका आश्रम समिति की भी स्थापना कर डाली।
इस आश्रम में बालिकाओं को ऐसे पढ़ाया जाता था, ताकि उनका इस तरह मानसिक विकास हो सके कि उनमें अपने पैरों पर खड़ा होने की भावना मज़बूत हो जाए। इस कार्य में गोपालकृष्ण गोखले का उन्हें भरपूर सहयोग मिला। लोकमंडल के कामों में ज़रा भी फुरसत मिलती, तो गोखले कर्वे जी के आश्रम में आते और सुधार के कार्यक्रमों पर बातचीत होती।
उनकी आलोचनाएं कम नहीं हुईं। इससे उनका मन बहुत दुखी हुआ। दिन-रात काम में लगे रहने के बाद भी सबको सन्तुष्ट नहीं कर पा रहे थे, फिर भी परेशान होकर रुके नहीं। वह आत्म-मन्यन करके अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश करते रहते।
कर्वे जी ने अपने पास की सारी जमा-पूंजी आश्रम को दान कर दी और अधिक धन इकट्ठा करने के लिए गुजरात तथा महाराष्ट्र के शहरों में घूमने लगे। इतने पर भी उनका मन नहीं माना और अपनी पांच हज़ार रुपए की बीमा पॉलिसी को भी आश्रम के लिए दे दिया।
सन् 1908 में उन्होंने निष्काम कर्म मठ की भी स्थापना कर डाली। इस संस्था का मूल मन्त्र था – समाज-सेवा ही हमारा ईश्वर है और उनकी सेवा करने में ही लाभ समझना हमारी श्रद्धा है। आगे चलकर इन तीनों संस्थाओं को एक ही नाम दे दिया गया, वह था महिला आश्रम।
यह उनकी अटूट मेहनत का नतीजा था कि चार वर्षों में ही इस संस्था के कोष में दो लाख सोलह हज़ार रुपए इकट्ठे हो गए। तभी बम्बई के विख्यात उद्योगपति विट्ठलदास दामोदर ठाकरसी ने इस आश्रम और विद्यापीठ के नाम पन्द्रह लाख रुपए कर दिए। अपनी माता के नाम पर उन्होंने इस महिला विद्यापीठ का नाम ‘श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठ’ रखा।
महात्मा गांधी कर्वे जी की इस सफलता को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। विश्वविद्यालय में स्वदेशी भाषा के माध्यम की योजना को भी उन्होंने पसन्द किया, किन्तु दूरदर्शी बापू ने एक प्रस्ताव रखा कि उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेज़ी वैकल्पिक विषय होना चाहिए। इस पर कर्वे जी ने नम्रतापूर्वक अपनी बात पर अड़े रहे, तो केवल उन्हीं की ख़ातिर गांधी जी ने झुकना स्वीकार कर लिया। कर्वे जी ने इंसान इंसान के बीच किसी प्रकार का भेदभाव नहीं माना।
वह सभी जातियों के इंसानों को एक मानते थे। अपने इन्हीं विचारों की परिकल्पना को साकार करने के लिए 1944 में उन्होंने ‘समता’ संघ की भी स्थापना की थी। 1942 में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय ने उन्हें डॉक्टर ऑफ़ लॉ की उपाधि प्रदान की थी। 1950 में देशवासियों ने उनको महर्षि अलंकरण से विभूषित किया। 1951 में पुणे में उन्हें डी. लिट्. की उपाधि दी गई और 1955 में उन्हीं के द्वारा स्थापित नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठ ने भी डी. लिट्. से सम्मानित किया।
सन् 1955 में भारत सरकार ने उन्हें ‘पद्मविभूषण’ की उपाधि से नवाजा। बम्बई विश्वविद्यालय ने भी 1957 में भी उन्हें डॉक्टर ऑफ़ लॉ की उपाधि दी। 26 जनवरी, 1958 को उन्हें भारत सरकार द्वारा भारतरत्न के सर्वोच्च अलंकरण से विभूषित किया गया। यह निष्काम कर्मयोगी एवं समाजसेवी 9 नवम्बर, 1962 को 105 वर्ष की आयु में परमात्मा में लीन हो गया।
 Narvilnews Whole world at one eyesight
Narvilnews Whole world at one eyesight